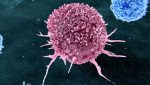साल 1992 की बात है, जब दिवंगत दार्शनिक गिलियन रोज़ उन बुद्धिजीवियों में शामिल थीं, जो पोलैंड के ‘कमीशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑशविट्स’ को सलाह दे रहे थे। यह वह दौर था जब पोलैंड, होलोकॉस्ट (नरसंहार) स्थल को यहूदी त्रासदी की बजाय पोलिश नुकसान के रूप में ज्यादा देख रहा था। रोज़ को यह सलाह देने का जिम्मा सौंपा गया था कि इस नरसंहार की यादों को हथियार बनाए बिना कैसे संजोया जाए।
रोज़ को जल्द ही अहसास हो गया कि यह एक छलावा है। उन्होंने महसूस किया कि अतीत की बुराइयों का सामना करने का यह प्रयास महज एक दिखावा बनकर रह सकता है। यह अत्याचार को याद करके खुद को सही साबित करने का एक आसान तरीका था, बजाय इसके कि उन परिस्थितियों की गहराई से जांच की जाए जो ऐसे अत्याचारों को जन्म देती हैं।
रोज के अनुसार, आयोग होलोकॉस्ट को एक “सुरक्षित पनाहगाह” (Safe Haven) में बदलने का जोखिम उठा रहा था, जहाँ हम अच्छाई और बुराई के सरल द्वंद्व में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
यह विचार आज भारतीय सिनेमा के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक हो जाता है। जब हम अपनी पीड़ा और अपमान का जश्न मनाते हैं क्योंकि हम उसके बाद मिलने वाली तथाकथित ‘जीत’ की मांग करते हैं, तो हम अनजाने में उसी मानसिकता का हिस्सा बन जाते हैं।
अपमान का प्रदर्शन और बदले की तैयारी
आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित ‘धुरंधर’ (2025) और ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ (2019) जैसी फिल्में पाकिस्तान के हाथों भारत के अपमान को बड़े चाव से पेश करती हैं। चाहे वह नागरिकों का गला रेतने के दृश्य हों, हाईजैक विमानों में कैद शरीर हों, या आत्मघाती हमलावरों द्वारा सैनिकों की शहादत।
ये दृश्य दर्शकों को उस “नॉकआउट पंच” या “घर में घुस के मारने” वाले पल के लिए तैयार करते हैं, जिससे उम्मीद की जाती है कि पुराना अपमान धुल जाएगा।
लेकिन जब कोई कथा वैचारिक (ideological) हो जाती है, तो सवाल नैतिकता का बन जाता है। क्या हम एक सुधरी हुई दुनिया चाहते हैं या सिर्फ प्रतिशोध वाली? जीत का आनंद अक्सर बार-बार अपमानित होने की आशंका पर टिका होता है।
धुरंधर: अपमानों की एक लंबी श्रृंखला
‘धुरंधर’, जो दो भागों वाली फिल्म श्रृंखला का पहला हिस्सा है, अपमानों की एक सूची प्रस्तुत करती है। फिल्म की शुरुआत IC-814 कंदहार हाईजैकिंग की भयावह तस्वीरों से होती है। इसके बाद 2001 का संसद हमला और फिर टीवी पर दिखाए गए 26/11 के दृश्य आते हैं। हर आतंकवादी घटना को एक अलग नजरिए से दिखाया गया है।
रणवीर सिंह फिल्म में एक भारतीय एजेंट ‘हमज़ा’ के रूप में नजर आते हैं, जो संसद हमले के बाद कराची के ल्यारी टाउन में गैंगवार में घुसपैठ करते हैं। ल्यारी कराची को नियंत्रित करता है, और कराची पाकिस्तान को। यह एक धीमा ऑपरेशन है, जहाँ ‘सब्र’ शब्द का बार-बार इस्तेमाल होता है। यह फिल्म ‘उरी’ के ठीक विपरीत है, जो त्वरित कार्रवाई पर आधारित थी। यहाँ परिणाम के लिए दर्शकों को अपमान के लंबे दौर से गुजरना पड़ता है।
विलेन का महिमामंडन और स्टाइल का खेल
चूंकि फिल्म का पहला भाग 3.5 घंटे लंबा है और असली बदला दूसरे भाग के लिए बचा कर रखा गया है, इसलिए धर को अपने नकारात्मक पात्रों को भी दिलचस्प बनाना पड़ा है। सारे पाकिस्तानी किरदार, विशेषकर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना), जो ल्यारी का सरगना है, को किसी हीरो जैसी एंट्री दी गई है।
वायरल हो चुका गाना “फसला या फासला” फिल्म की दुविधा को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ दक्षिणपंथी धड़ा इस बात से चिंतित है कि फिल्म पाकिस्तानी किरदारों का महिमामंडन कर रही है, वहीं बलोच लोग इस बात से नाराज हैं कि गीतों में अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। विलेन को हीरो जैसा ‘स्टाइल’ दिया गया है, लेकिन उनके पास हीरो जैसी नैतिकता नहीं है। क्या यह संभव है? यही ‘धुरंधर’ की सबसे बड़ी चुनौती है।
हिंसा के दो चेहरे
‘धुरंधर’ में हिंसा दो प्रकार की है।
- भारतीयों पर हिंसा: कंदहार हाईजैकिंग में गला रेतने या संसद हमले में महिला पुलिसकर्मी को गोली मारने के दृश्य। ये दृश्य स्पष्टता के साथ दिखाए गए हैं ताकि दर्शक सहानुभूति और बेबसी महसूस करें।
- वीभत्स हिंसा (Gore): खाल उधेड़ना, लोहे की कीलों पर फेंकना या सिर को बुरी तरह कुचलना। यह हिंसा इतनी क्रूर है कि आप स्क्रीन से नजरें हटाना चाहेंगे। इसमें न तो मरने वाले के लिए सहानुभूति है और न ही मारने वाले के लिए कोई औचित्य।
भविष्य की आहट और राजनीतिक संदेश
यह फिल्म सिर्फ अतीत का चित्रण नहीं है, बल्कि एक भविष्य का आह्वान भी है। फिल्म लगातार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को देश के भविष्य के रक्षकों के रूप में संकेत देती है। 2000 के दशक में सेट की गई इस फिल्म में पात्र उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब कोई मजबूत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आएगा जो पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगा।
फिल्म तथ्यों के साथ खेलती है। यह भारत की खुफिया जानकारी और पाकिस्तान के गैंगवार के पात्रों को लेकर एक काल्पनिक कहानी बुनती है, लेकिन यह वास्तविकता के इतना करीब है कि लोग समझ सकें कि इशारा किसकी तरफ है। सरल शब्दों में कहें तो यह वर्तमान प्रशासन की प्रशंसा करने के लिए रचा गया एक सिनेमाई प्रयास है, जिसे कई आलोचक ‘प्रोपेगेंडा’ कह रहे हैं।
नोटबंदी (Demonetisation) को पहले भाग में इतना बिल्ड-अप दिया गया है कि संभवतः दूसरे भाग में इसे एक नायक की तरह पेश किया जाएगा।
क्या हम स्टाइल और नैतिकता को अलग कर सकते हैं?
फिल्म ‘आर्टिकल 370’ (2024) की तरह, ‘धुरंधर’ भी यह तर्क देती है कि “आतंकवाद सिर्फ एक बिजनेस है, इसका आजादी के ड्रामे से कोई लेना-देना नहीं है।” फिल्म शुरू में बलोच विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति दिखाती है, लेकिन अंततः उन्हें भी पैसे के लिए काम करने वाले व्यापारियों में बदल देती है।
सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय राय यह है कि ‘धुरंधर’ जैसी फिल्में “अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा” हैं और हमें इनकी सम्मोहक शैली (Slick Style) से सावधान रहना चाहिए। सुसान सोनटैग ने अपने 1975 के निबंध “फैसिनेटिंग फासीवाद” में तर्क दिया था कि हम ‘फासीवादी सौंदर्यशास्त्र’ (Fascist Aesthetics) को उसकी विचारधारा से अलग नहीं कर सकते।
आज भारत में फिल्म के ट्रेलर ही सांस्कृतिक दस्तावेज बन गए हैं। ‘उरी’, ‘धुरंधर’ और ‘आर्टिकल 370’ जैसी फिल्में तकनीकी रूप से बेहतरीन हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उनकी चमक-दमक का आनंद लेते हुए उनके जहरीले संदेश को नजरअंदाज कर सकते हैं? यह फिल्म से ज्यादा हमारे अपने विवेक की परीक्षा है। हमें फिल्म से नहीं, बल्कि अपनी खुद की उस इच्छा से डरना चाहिए जो ऐसे आख्यानों में सुकून तलाशती है।
यह भी पढ़ें-