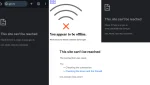मुझे पूरी उम्मीद थी कि 2 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के दिल्ली दंगा मामले में 18 में से 9 अभियुक्तों की ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के अंतर्निहित अन्याय के खिलाफ एक ज़ोरदार आवाज़ उठेगी। मेरी यह आशा उस जन-आक्रोश से उपजी थी जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली और आसपास के शहरों के नगर निगमों को आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाने के आदेश के खिलाफ व्यक्त किया गया था।
लेकिन मेरी उम्मीदें टूट गईं। मैं यह सिर्फ़ कड़वाहट में नहीं कह रहा हूँ: ऐसा लगता है कि भारत में मुसलमानों की तुलना में कुत्तों के लिए न्याय पाने की संभावना बेहतर है।
आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाने के आदेश पर उठे भारी बवाल ने शायद सुप्रीम कोर्ट को 11 अगस्त के अपने आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए प्रेरित किया।
महज़ 11 दिनों के भीतर, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी, डीवर्मिंग और टीकाकरण के बाद उन्हीं इलाकों में वापस छोड़ा जाना चाहिए जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था। शीर्ष अदालत ने जिसे “आवारा कुत्तों का सड़कों पर रहने का अधिकार” और “नागरिकों की सुरक्षा” कहा, उसके बीच संतुलन बनाने में सिर्फ़ 11 दिन का समय लिया।
कुत्तों को न्याय देने में सुप्रीम कोर्ट की यह तत्परता, दिल्ली दंगा मामले में नौ अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाओं से निपटने में अदालतों की कछुआ चाल के बिल्कुल विपरीत है। ये नौ लोग पिछले पाँच सालों से जेल में हैं और इस दौरान उनकी ज़मानत याचिकाएँ विभिन्न अदालतों में एक बेंच से दूसरी बेंच पर घूमती रहीं।
कई बार न्यायाधीशों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, या फिर दलीलें सुनने के बाद महीनों तक कोई आदेश पारित नहीं किया और उनका तबादला हो गया, जिससे ज़मानत की प्रक्रिया फिर से शून्य से शुरू करनी पड़ी।
ये नौ कार्यकर्ता उन 18 लोगों में शामिल हैं, जिन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सरकार के अनुसार, यह विरोध प्रदर्शन फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की एक साजिश थी, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई थी। क्या मौतों का यह आंकड़ा उनकी ज़मानत याचिकाओं की धीमी प्रगति के पीछे एक कारण हो सकता है? क्या अदालतें उन्हें राहत देने में इसलिए झिझक रही थीं कि इससे जनभावनाएँ आहत हो सकती हैं?
इस मामले में कुत्ते उन नौ कार्यकर्ताओं की तुलना में कहीं ज़्यादा भाग्यशाली हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2024 में देश भर में कुत्ते के काटने के 37.17 लाख मामले सामने आए और “कई मामलों में, सदमे और रेबीज संक्रमण के कारण लोगों की जान चली गई।” इसके बावजूद, उन्हें सड़कों से स्थायी रूप से हटाने के आदेश ने एक बड़े सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा “दयालु व्यवहार” के आधार पर उस आदेश को पलटने के साथ ही शांत हो गया।
अदालतों के लिए भी यह एक दयालुतापूर्ण कदम होता अगर वे इन नौ कार्यकर्ताओं को रिहा कर देतीं, क्योंकि उनका मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मामले में 800-900 गवाहों से पूछताछ होनी है, ऐसे में उनकी सज़ा तय होने में सालों लग जाएँगे। क्या न्यायपालिका को, जैसा कि उसने कुत्तों के लिए किया, इन कार्यकर्ताओं के स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य और लोगों की सुरक्षा के साथ संतुलित नहीं करना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के साथ दयालु व्यवहार का एक अपवाद भी बताया – वे कुत्ते जिन्हें रेबीज है, उन्हें अलग-थलग किया जाना चाहिए। इसी तरह, “जेल नहीं, ज़मानत” एक मार्गदर्शक न्यायिक सिद्धांत है। UAPA के तहत भी एक अपवाद है – किसी अभियुक्त को ज़मानत से वंचित किया जाना चाहिए यदि अदालत को लगता है कि उसके खिलाफ आरोप पहली नज़र में (prima facie) सच है।
सुप्रीम कोर्ट ने वटाली मामले में फैसला सुनाया था कि यदि कोई न्यायाधीश अभियुक्त के खिलाफ सबूतों की विश्वसनीयता की जाँच करता है, तो यह पहली नज़र में सच नहीं माना जाएगा। ‘प्राइमा फेसी’ का मतलब यह तय करना है कि क्या राज्य की कहानी पहली छाप में ही झूठी लगती है – यानी, बिना गहराई से विश्लेषण किए।
वटाली मामले ने एक झटके में इंसानों और आवारा कुत्तों को एक ही पायदान पर खड़ा कर दिया, क्योंकि यह पता लगाने के लिए कोई निश्चित परीक्षण नहीं है कि किसी कुत्ते को रेबीज है या नहीं। उनमें केवल लक्षणों के आधार पर रेबीज होने का संदेह किया जा सकता है, जैसे कि अचानक और अकारण आक्रामकता।
कुत्तों में रेबीज का निदान अनिवार्य रूप से एक ‘प्राइमा फेसी’ निर्धारण है – और यह गलत भी हो सकता है। लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि कोई पूर्वाग्रह या दुर्भावना से किसी कुत्ते को रेबीज से पीड़ित घोषित कर दे।
मुसलमान इस मामले में दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ राज्य ने उनके खिलाफ सबूत गढ़े हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को रिहा करना है। हाई कोर्ट ने माना कि उनसे कबूलनामे निकलवाने के लिए उन्हें “अमानवीय यातना” दी गई थी और गवाहों के बयान अविश्वसनीय थे। ये सभी 11 लोग, जो मुस्लिम थे, 19 साल जेल में बिता चुके थे।
स्वतंत्रता के ऐसे दुखद हनन से बचने के लिए ही यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य अपने आरोपों के समर्थन में जो सबूत पेश करता है, उनके मूल्य को स्थापित करने के लिए एक सतही विश्लेषण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया ने 2023 में भीमा कोरेगांव मामले के अभियुक्तों वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को ज़मानत देने के लिए यही किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में सबूतों का शायद ही कोई सतही विश्लेषण किया। अब जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो यह उम्मीद की जाती है कि दयालु व्यवहार और परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच सामंजस्य के जो न्यायिक सिद्धांत कुत्तों पर लागू किए गए थे, वे उन नौ मुस्लिम कार्यकर्ताओं पर भी लागू होंगे, जिनका विरोध उनकी समझदारी का प्रतीक था, न कि किसी पागलपन का।
नोट- लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और भीमा कोरेगांव: चैलेंजिंग कास्ट के लेखक हैं।
यह भी पढ़ें-
“क्या यह भारत नहीं है?” – जब पंजाब पुलिस ने राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावित गांव जाने से रोका
वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट, SIT जांच में सभी आरोप खारिज